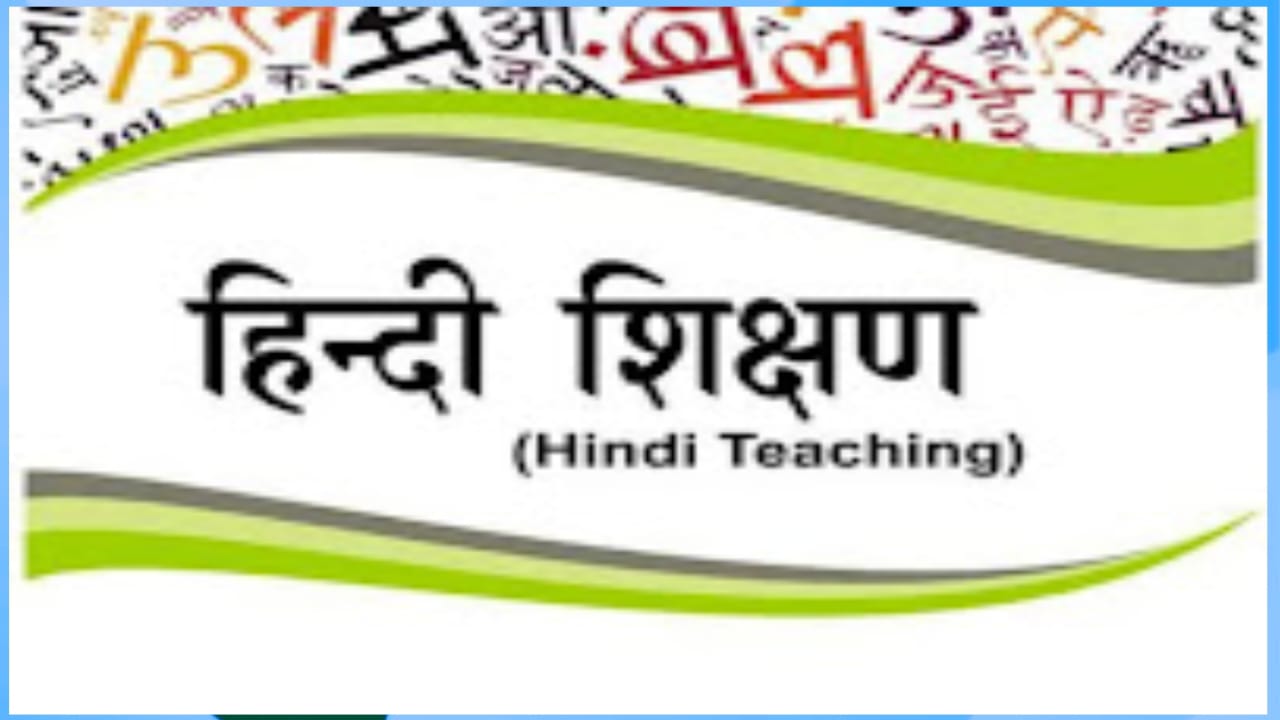2. उच्चारण कौशल
उद्देश्य और महत्त्व –
समाज में सामंजस्य बनाने हेतु। राजनीति में प्रतिष्ठा प्राप्त ज्ञानेन्द्रियों का विकास करने हेतु।
दूसरों की नजरों में अपनी छवि बनाने हेतु।
– शिष्ट आचरण को दिखाने हेतु।
उच्चारण कौशल की मुख्य विधियाँ –
1. वाद – विवाद
2. भाषण
3.अंत्याक्षरी
3. वाचन कौशल
वाचन का अर्थ – पढ़ना होता है। इसमें बालकों को किसी भी लिखे हुए अंश को पढ़ने योग्य बनया जाता है।
उद्देश्य और महत्त्व –
1. बालकों को शुद्ध पढ़ना सिखाना।
2. बालकों में किसी भी लिखे हुए लेख को पढ़ने की क्षमता उत्पन्न करना।
वाचन शिक्षण की मुख्य विधियाँ
1. देखों और कहो विधि- इस विधि में बालकों को अध्यापक अक्षरों का ज्ञान न कराकर शब्दों का ज्ञान कराता है।
अभ्यास – कमल, नयन
2. अक्षर बोध विधि – इस विधि में अध्यापक बालकों को शब्दों का बोध न कराकर अक्षर बोध कराता है।
अभ्यास – कमल
3. ध्वनि साम्य विधि- इस विधि में अध्यापक एक समान उच्चारित होने वाले शब्दों को एक साथ सिखाता है।
अभ्यास – कर्म, धर्म, मर्म
4. अनुध्वनि विधि
इस विधि में अध्यापक बालकों से ध्वनि का अनुकरण करने के लिए कहता है तथा वह शब्द जिन्हें लिखा कुछ और जाता है और पढ़ा कुछ और जाता है उसमें अनुध्वनि का प्रयोग किया जाता है।
अभ्यास – 1. PUT उ
2. BUT अ
5. संगति/साहचर्य विधि – साहचर्य का अर्थ समानता दर्शाना होता है ।
~ साहचर्य विधि की जनक इटली की मैडम /मरियम मेन्टेसरी है।
~ इस विधि में शब्दों को उनके चित्रों के साथ या नामों को उनके चित्रों के साथ समानता दर्शायी जाती है।
~ इसमें भाषा की इकाई शब्द को माना गया है।
6. भाषा यंत्र उपकरण विधि – इस विधि में अध्यापक 4 प्रकार के उपकरणों का उपयोग करता है।
– टेपरिकॉर्डर
– कैसिट
– सहायक चित्र
– सहायक पुस्तक
7. समवेत् पाठ विधि – इसमें अध्यापक और बालक दोनों मिलकर पाठ का वाचन करते है।

मुख्य रूप से
~ मौन वाचन से बालकों की वर्तनी संबंधी/उच्चारण संबंधी दूर नहीं होती है।
~ मौन वाचन बालकों में चिंतनशीलता का विकास करता है।
~ गहन वाचन से बालकों में एकाग्रता का विकास होता है।
~ तीव्र वाचन से बालकों की पठन गति का विकास होता है।
~ संकोची प्रवृत्ति के बालकों के लिए समवेत् वाचन/सामूहिक वाचन उपयोगी है।
लेखन कौशल
उद्देश्य और महत्त्व
– बालकों को शब्दों को शुद्ध लिखने की योग्यता प्रदान करना।
– इसमें बालकों की ज्ञानेन्द्रियाँ सक्रिय रहती है।
– बालक शब्दों को सही-सही व उचित प्रकार से लिखना सीखता है।
लेखन कौशल की 5 विधियाँ हैं –
1. रूप रेखा अनुकरण विधि – इसमें अध्यापक बालकों की अभ्यास पुस्तिका में बिंदुओं की सहायता से या अपने हल्के हाथों से आकृति बनाता है और फिर बालकों से उन्हीं बिंदुओं पर या रेखाओं पर कलम घुमाने के लिए कहा जाता है। बालक इन हल्की रेखाओं को पुष्ट करके/गहरा करके शब्दों को लिखना सीखता है।
~ वर्तमान में इस विधि के लिए कई अभ्यास पुस्तिकाएँ भी उपलब्ध है यह प्राचीन विधि है ।
2. स्वतंत्र अनुकरण विधि – इस विधि में अध्यापक बालकों की अभ्यास पुस्तिका में शब्दों को लिखता है और फिर बालकों से उन्हीं शब्दों का अनुकरण करने के लिए कहा जाता है।
3. मोन्टेसरी विधि – बालक ही आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर मैडम मोन्टेसरी ने इस विध का निर्माण किया।
~ इसमें कागज के मोटे गत्तों, लकड़ी व प्लास्टिक के टुकड़ों पर शब्दों की उभरी हुई आकृति होती है।
~ बालकों को इन आकृतियों पर अंगुली घुमाने के लिए कहा जाता है ।
~ फिर उन्हें शब्दों का ज्ञान कराया जाता है।
~ इस विधि में बालकों के हाथ, आँख और कान तीनों सक्रिय रहते है ।
4. पैस्टोलॉजी विधि – इस विधि में अध्यापक वर्णो के टुकड़े करके फिर उन टुकड़ों को मिलाकर अक्षरों का ज्ञान कराता है।
अभ्यास – क – 0, | क्, क
5. जेकोटॉट विधि
~ जेकोटॉट महोदय के नाम पर ही इस विधि का नाम जेकोटॉट रखा गया।
~ इस विधि में अध्यापक द्वारा श्यामपट्ट पर लिखे हुए मूल शब्द को देखकर बालक अपने लिखे हए शब्द में संशोधन करता है।
~ यह विधि बालक को स्वयं संशोधन करने का मौका देती है।
पाठ्यपुस्तक
अंग्रेजी के Book शब्द की उत्पत्ति जर्मन भाषा के Beach शब्द से मानी जाती है। जिसका अर्थ वृक्ष होता है। फ्रांसीसी/भाषा में भी इस शब्द का अर्थ वृक्ष की छाल/तख्ती पर लिखने से है।
~ पाठ्यपुस्तक में विषयवस्तु का प्रस्तुतीकरण सरल-कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर व स्थूल से सूक्ष्म की ओर होना चाहिए।
~ पाठ्यपुस्तक की आवश्यकता पाठ्यपुस्तक शिक्षण का साधन है, साध्य नहीं इसके माध्यम से शिक्षा के विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है।
~ पाठ्यपुस्तक पाठ्यक्रम निर्माण में सहायक है।
पाठ्यपुस्तक की आवश्यकता अध्यापक व बालक दोनों को होती है।
~ पाठ्यपुस्तक से ज्ञानार्जन में सहायता मिलती है।
~ पाठ्यपुस्तक में सूचनाओं का संग्रह होता है।
~ पाठ्यपुस्तक से बालकों को गृहकार्य करने में सहायता मिलती है ।
~ पाठ्यपुस्तक से विषयवस्तु को पुनः स्मरण करने में सहायता मिलती है।
पाठ्यपुस्तक के गुण(स्थूल – सूक्ष्म)
1. स्तरानुकूल
2. व्यवहारिकता
3. शुद्धता
4. मूल्य
5. मुद्रण
6. कागज
उपागम, शिक्षण अधिगम सामग्री सहायता सामग्री, लघुमाध्यम शिक्षण के अन्य संसाधन उपागम – शिक्षण में सुधार लाने के लिए, शिक्षण को बालकों के लिए सरल, रोचक व प्रभावी बनाने के लिए जिन साधनों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें ही उपागम कहते हैं।
सहायता सामग्री/शिक्षण-अधिगम सामग्री – वह सामग्री जिसके माधयम से बालक सीखते है, सहायक सामग्री कहलाती है।
~ दूसरे शब्दों में वह सामग्री जिसके माध्यम से शिक्षण को प्रभावी बनाया जाए शिक्षण अधिगम सामग्री कहलाती है। यह 3 प्रकार की होती है।
1. श्रव्य सामग्री – टेपरिकॉर्डर, रेडियो, ग्रामोफोन, लिंग्वाफोन
2. दृश्य सामग्री – चार्ट, मॉडल, मानचित्र, श्यामपट्ट (परंपरागत शिक्षण अधिगम) प्रोजेक्ट, चित्र विस्तारक यंत्र (एपिडायस्कोप) प्रत्यक्ष वस्तुएँ, स्लाइड्स, ओवरहेड प्रोजेक्टर आदि।
3. दृश्य सामग्री – दूरदर्शन, कम्प्यूटर, डॉक्यूमेन्ट्री फिल्म, वीडियो टेप आदि।