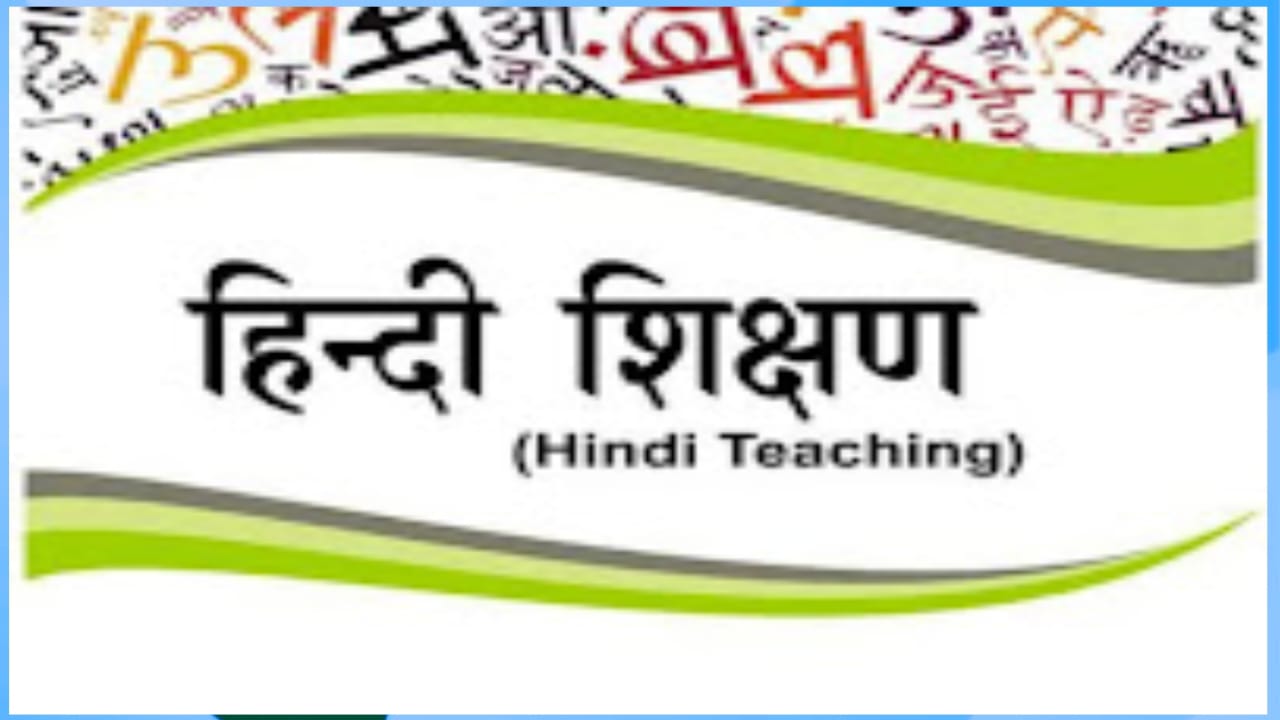प्रत्यक्ष विधि
- ~ प्रत्यक्ष का अर्थ होता है – आँखो के सामने घटित होना।
- ~ 17वीं सदी में ‘जॉन कमेनियस’ ने यह विचार रखा कि भाषा को व्यावहारिकता के आधार पर सिखाया जाना चाहिए इस प्रकार द्वितीय भाषा-शिक्षण के लिए व्याकरण अनुवाद विधि के स्थान पर किसी अन्य विधि की आवश्यकता सबसे पहले जॉन कमेनियल ने महसूस की।
- ~ व्याकरण अनुवाद विधि के दोषों को दूर करने के लिए इसे लाया गया।
- ~ प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग सबसे पहले फ्रांस में 1901 में अंग्रेजी भाषा शिक्षण के लिए किया गया।
- ~ भारत में यह विधि 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में आई। इसे बंगाल में लाने वाले श्री टीपिंग थे। मुंबई में लाने वाले श्री फ्रेजर थे। मद्रास में लाने का श्रेय श्री येट्स को जाता है।
- ~ प्रत्यक्ष विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि जिस प्रकार बालक श्रवण व अनुकरण के माध्यम से अपनी मात्र भाषा सीखता है। उसी प्रकार वह द्वितीय भाषा भी सीख सकता है।
- ~ व्याकरण की अलग से पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है।
- ~ हर वस्तु को कक्षा-कक्ष में प्रत्यक्ष ला पाना संभव नहीं होता। प्रत्यक्ष विधि के द्वारा संज्ञा शब्दों का बोध तो कराया जा सकता है। परंतु मन के भावों का बोध करा पाना संभव नहीं होता है।
- अनुकरण/अनुकरणात्मक विधि
- ~ शिक्षण जैसा बोले वैसी ही नकल करना अनकरण कहलाता है। इस विधि में बालक को प्रारंभ में अक्षर ज्ञान कराया जाता है।
- ~ यह विधि प्राथमिक स्तर पर प्रभावी है इसमें बालक शिक्षक का अनुकरण कर बोलना (उच्चारण) करना, लिखना वह रचना करना सीखता है।
- ~ यह विधि प्राथमिक स्तर पर लिखना व बोलना सिखाती है तथा माध्यमिक स्तर पर रचना करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है।
- ~ इस विधि में तीन प्रकार का अनुकरण होता है।
- 1. उच्चारण अनुकरण
- 2. लेखन अनुकरण
- 3. रचना अनुकरण
1. उच्चारण अनुकरण – शिक्षक जैसा बोले, बालक के द्वारा उसकी ध्वनियों का वैसा ही अनुकरण किया जाए तो उसे उच्चारण अनुकरण कहते है।
2. लेखन अनुकरण – शिक्षक के द्वारा लिखे हए शब्दों का वैसा ही अनुकरण करना लेखन अनुकरण कहलाता है।
3. रचना अनुकरण – इस अनुकरण में अध्यापक बालकों के सामने एक रचना प्रस्तुत करता है और बालकों से उसी रचना का अनुकरण कर एक नवीन रचना लिखने के लिए कहा जाता है। इस अनुकरण में भाषा तो बालक की होती है परंतु उसे शैली के अध्यापक द्वारा बताई जाने वाली रचना पर ही निर्भर रहना पड़ता है |

1. श्रवण कौशल
उद्देश्य और महत्त्व–
इसमें बालकों की ज्ञानेन्द्रियों का विकास होता है। बालकों में श्रवण के प्रति जागरूकता पैदा होती है। श्रवण कौशल की मुख्य विधियाँ निम्नलिखित है
– श्रुतलेखन अभ्यास विधि इस विधि में अध्यापक बोलता है और बालक उसे सुनकर लिखते हैं। इस विधि में बालकों के श्रवण कौशल और लेखन कौशल दोनों का विकास होता है। श्रुतलेखन के माध्यम से बालकों की वर्तनी व वर्णागति संबंधी अशुद्धियों को दूर किया जाता है। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का 10-15 प्रतिशत समय श्रुतलेखन के लिए रखा गया है। तथा उच्च स्तर पर यह समय 3-5 प्रतिशत रखा गया है। प्राथमिक स्तर के लिए पठित अंश का तथा उच्च स्तर के लिए अपठित अंश का श्रुतलेख लेना लाभकारी होता है। इस विधि में अध्यापक पूरे अंश को तीन बार बोलकर सुनाता है।
वाद – विवाद :- इसमें अध्यापक की भूमिका गौण होती है। वाद-विवाद में किसी भी विषयवस्तु के पक्ष तथा विपक्ष में चर्चा की जाती है। और बालक श्रवण कौशल के माध्यम से उस वाद-विवाद को बहुत ध्यान से सुनते है।भाषण भाषण देना भी अपने आप में कला है। भाषण जितना ज्यादा प्रभावी होगा। श्रोताओं पर उसका उतना ही असर होगा।
कविता पाठ:- कविता पाठ में अध्यापक बालकों को उतार – चढ़ाव का ध्यान रखते हुए कविता पाठ करके सुनाता है। और बालक भी शिक्षक को सुनकर उसी उतार-चढ़ाव के साथ कविता पाठ करते हैं।
सस्वरपाठ :- यह पाठ कविता पढ़ाने के लिए उपयुक्त है। इसमें अध्यापक उचित लय व ताल के साथ स्वरों का ध्यान रखते हुए कविता पाठ करते है और बालक भी उन्हें सुनकर वैसा ही अनुकरण करते हैं।
अंत्याक्षरी :- इसमें बालकों के दो समूह होते हैं, इसमें कविता का अंतिम अक्षर जहाँ खत्म होता है, उसी अक्षर से दूसरा समूह नई कविता सुनाता है।