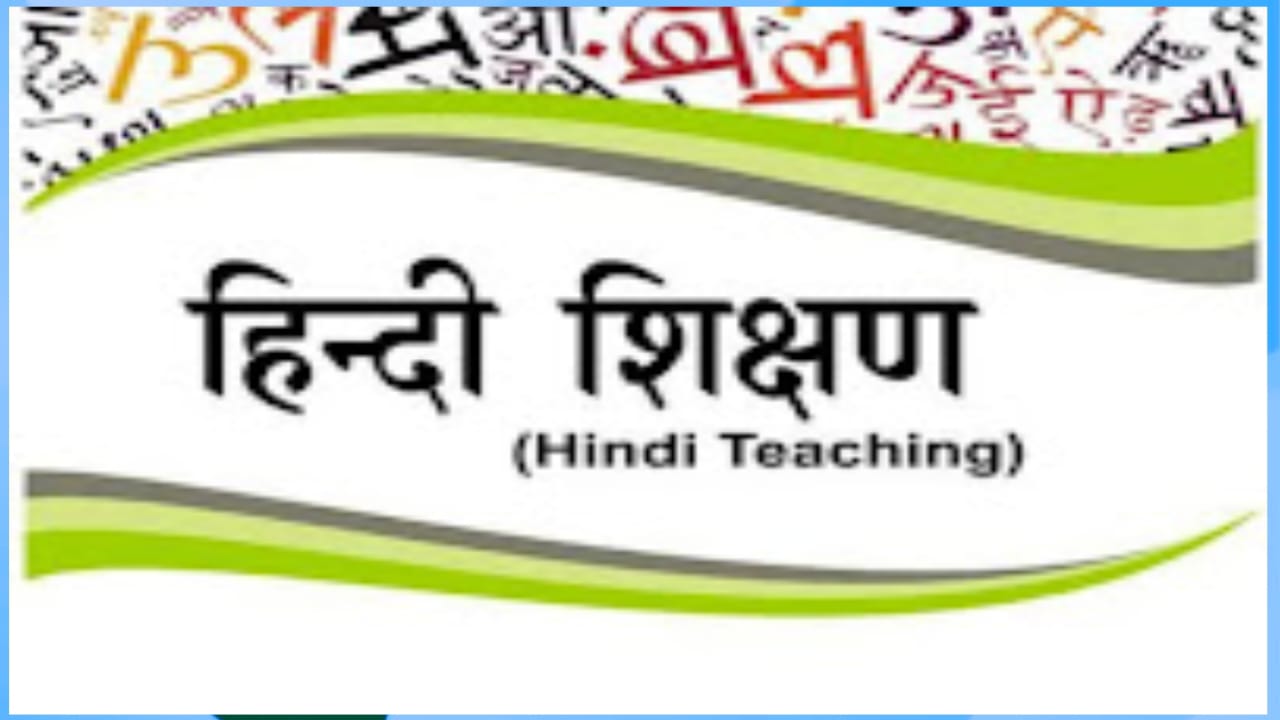कहानी शिक्षण की विधियाँ
1. कथन विधि
2. कक्षा अभिनय विधि
3. चित्र विधि
4. प्रश्नोत्तर/खंडान्वय विधि
5. वार्तालाप
कथन विधि- कहानी का कथन जितना ज्यादा प्रभावीशाली होगा बालकों को उतने ही अच्छे तरीके से अधिगम होगा। कथन करना भी अपने आप में एक कला है। अध्यापक कथन के माध्यम से पूरी कहानी सुना देता है। इसमें सिर्फ अध्यापक ही सक्रिय रहता है। अमनोवैज्ञानिक विधि है।
कक्षा अभिनय विधि- यदि किसी कहानी में पात्र हैं तो अध्यापक बालकों के द्वारा उन पात्रों का अभिनय कक्षा में करवाता है और यदि पात्र नहीं है तो अध्यापक चेहरे की भाव भंगिमाओं के माध्यम से व हाथों के संकेतों के माध्यम से कहानी का अभिनय प्रस्तुत करता है। मनोवैज्ञानिक विधि है।
चित्र विधि- इस विधि में अध्यापक क्रम से एक-एक चित्र को प्रस्तुत करता है और चित्रों के माध्यम से बालकों से प्रश्न करता है इसमें चित्रों के द्वारा अध्यापक पूरी कहानी को बालकों के सामने प्रस्तुत कर देता है। मनोवैज्ञानिक विधि है।
प्रश्नोत्तर विधि- इस विधि में अध्यापक प्रश्नों के माध्यम से बालकों को पूरी कहानी सुना देता है। मनोवैज्ञानिक विधि है।
वार्तालाप/संवाद विधि- इस विधि में कहानी में आने वाले पात्रों के बारे में व कहानी के बारे में अध्यापक बालकों से वार्तालाप करता है।
नाटक शिक्षण की विधियाँ
1. रंगमंच अभिनय प्रणाली
2. व्याख्या प्रणाली
3. आदर्श नाट्य शिक्षण प्रणाली
4. संयुक्त प्रणाली
5. कक्षा अभिनय प्रणाली
रंगमंच अभिनय प्रणाली– इस प्रणाली में नाटक का प्रस्तुतीकरण रंगमंच पर किया जाता है। कक्षा के अतिरिक्त खंडो में व अतिरिक्त धन के साथ नाटक को रंगमंच पर प्रस्तुत किया जाता है। इसे समय साध्य तथा व्यय साध्य विधि भी कहा जाता है। सभी विद्यालय इसे कर पाने में सक्षम नहीं हो पाते हैं।
व्याख्या प्रणाली- इस प्रणाली में अध्यापक नाटक में आने वाले पात्रों के बारे में उद्देश्यों के बारे में, प्रस्तुतीकरण के बारे में व्याख्या करके बताता है। मनोवैज्ञानिक विधि है।
आदर्श नाट्य शिक्षण प्रणाली- इस प्रणाली में संपूर्ण भागीदारी शिक्षक की होती है। छात्र तो दर्शक व श्रोता के रूप में सुनते हैं, इसमें अध्यापक का उद्देश्य बालकों का मनोरंजन करना होता है।
संयुक्त प्रणाली- इसे नाटक शिक्षण की आदर्श प्रणाली कहा जाता है। यह आदर्श नाट्य शिक्षण प्रणाली और कक्षा अभिनय प्रणाली दोनों का सम्मिलित रूप है इसमें अध्यापक व बालक दोनों मिलकर नाटक का प्रस्तुतीकरण करता है।
कक्षा अभिनय प्रणाली- इस विधि में कक्षा में ही बालक के द्वारा नाटक का प्रस्तुतीकरण किया जाता है। मनोवैज्ञानिक विधि है।
पद्य शिक्षण
कविता शिक्षण की विधियाँ-
1. अभिनय प्रणाली
2. तुलना प्रणाली
3. गीत प्रणाली
4. अर्थ बोध विधि
5. समीक्षा प्रणाली
6. रसास्वादन विधि
7. व्यास विधि
8. प्रश्नोत्तर विधि/खण्डान्वय विधि व्याख्या विधि
1. अभिनय प्रणाली- इस प्रणाली में अध्यापक हाथों के संकेतों के माध्यम से व चेहरे के भावों के माध्यम से कविता को प्रस्तुत करता है फिर बालकों से वैसा ही अनुकरण करवाता है। — यह प्राथमिक स्तर पर प्रभावी है। मनोवैज्ञानिक
2. तुलना प्रणाली- इस प्रणाली में अध्यापक प्रस्तुत कविता के समान कोई दूसरी कविता/ उसी कवि द्वारा लिखित कोई अन्य कविता बालकों के सामने प्रस्तुत करता है। इससे बालकों के ज्ञान व उनकी तर्कशक्ति में वृद्धि होती है। यह उच्च स्तर पर प्रभावी है। मनोवैज्ञानिक विधि है।
3. गीत प्रणाली- यह कविता शिक्षण की सबसे उत्तम प्रणाली है। इसका उद्देश्य कविता में आने वाले उतार – चढ़ाव का ध्यान रखते हुए लय व ताल के साथ कविता का सस्वर वाचन करना है। मनोवैज्ञानिक विधि है। यह प्राथमिक स्तर पर प्रभावी है।
4. अर्थबोध विधि- यह माध्यमिक स्तर पर प्रभावी है। अमनोवैज्ञानिक विधि है।
5. समीक्षा प्रणाली- कविता का वास्तविक मूल्यांकन समीक्षा प्रणाली में किया जाता है। इसमें कविता को आलोचना की कसौटी पर कसा जाता है। यह उच्च स्तर के बालकों के लिए प्रभावी है।
6. रसास्वादन विधि- रसास्वादन विधि का प्रयोग कविता पाठ करने में किया जाता है। मनोवैज्ञानिक विधि है। इस विधि का उद्देश्य बालकों को रस व आनंद की प्राप्ति करने में सक्षम बनाना है। प्राचीन समयस में किसी भी बात को स्मृति में अंकित करने के लिए उसे कविता का रूप दे दिया जाता था। जिससे कि वह जानकारी कभी विस्मृत नहीं होती यह प्राथमिक स्तर पर प्रभावी है। यह प्राथमिक स्तर पर प्रभावी है।
7. व्यास प्रणाली व्यास का अर्थ कथावाचन होता है। इस प्रणाली में अध्यापक कविता की व्याख्या करने के साथ-साथ उसमें आने वाले एक-एक शब्द की उपयोगिता, शब्द विन्यास, विगृह आदि के बारे में बताता है। भावात्मक कविताओं को पढ़ाने में इसी प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। इसमें अध्यापक को कविता की गहनतम जानकारी होना अत्यन्त आवश्यक होता है। यह माध्यमिक स्तर पर प्रभावी है। व्यास प्रणाली को व्याख्या प्रणाली का विस्तृत रूप कहा जाता है। अमनोवैज्ञानिक विधि है।
8. व्याख्या प्रणाली इस प्रणाली में अध्यापक कविता में आने वाले रस, छंद, अलंकार आदि की व्याख्या करके बताता है। यह माध्यमिक स्तर पर प्रभावी है। अमनोवैज्ञानिक विधि है।
9. प्रश्नोत्तर/खण्डान्वय प्रणाली वर्णात्मक व ऐतिहासिक पद्यों को पढ़ाने के लिए प्रश्नोत्तर प्रणाली का सहयोग लिया जाता है। इसमें कविता के खंडो को मिलाकर बालकों से प्रश्न किए जाते हैं। इसलिए इसके प्रश्नोत्तर व खंडान्वय प्रणाली कहा जाता है। यह माध्यमिक स्तर पर प्रभावी है। मनोवैज्ञानिक विधि है।
व्याकरण शिक्षण की विधियाँ
1. व्यतिरेक विधि
2. व्याकरण अनुवाद विधि
3. पाठ्यपुस्तक प्रणाली
4. आगमन विधि
5. समवाय विधि
6. सूत्र विधि
7. निगमन
8. भाषा संसर्ग/अव्याकृति
1. व्यतिरेक विधि — व्यतिरेक का अर्थ – विभेद/तुलना करना होता है। यह द्वितीय भाषा शिक्षण की विधि है। इसे तुलनात्मक विधि का नाम से भी जाना जाता है।
— इस विधि में व्याकरण ज्ञान अध्ययन के साथ ही चलता है।
— इसमें प्रथम भाषा व द्वितीय भाषा में समानता को याद न कराकर बालकों को असमानताओं को याद कराया जाता है।
2. व्याकरण अनुवाद विधि — इस विधि के प्रवर्तक ‘डॉ. रामकृष्ण गोपाल भण्डारकर’ हैं। इसे भण्डारकर विधि के नाम से भी जाना जाता है। द्वितीय भाषा शिक्षण की यह सर्वाधिक प्रचलित व प्राचीनतम विधि है। इस विधि में बालकों को सबसे पहले द्वितीय भाषा की व्याकरण पढ़ाई जाती है। फिर द्वितीय भाषा के नियमों के बारे में बताया जाता है। इसके पश्चात् प्रथम भाषा का अनुवाद द्वितीय भाषा में कर दिया जाता है।
— इसमें बालक का सैद्धांतिक पक्ष तो मजबूत हो जाता है परंतु बालक का व्यावहारिक पक्ष कमजोर रह जाता है।
— यह विधि अनुवाद के सिद्धांत पर आधारित है।
— द्वितीय भाषा शिक्षण की स्वयं शिक्षण मालाएँ भी इसी विधि पर आधारित है।
3. पाठ्यपुस्तक प्रणाली — इसे तोता रटन्त प्रणाली, सुगम प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है।
— इसमें बालकों को पाठ्यपुस्तक में आने वाले (बड़े-बड़े) नियमों को रटा दिया जाता है।
4. आगमन विधि उदाहरण
– नियम की ओर मूर्त
– अमूर्त की ओर विशष्टि
– सामान्य की ओर स्थूल
– सूक्ष्म की ओर ज्ञात
– अज्ञात की ओर — आगमन विधि को सहयोग प्रणाली, प्रयोग प्रणाली व सहसंबंध प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। — आगमन विधि बालक-केन्द्रित विधि है।
5. निगमन विधि नियम
- – उदाहरण की ओर अमूर्त
- – मूर्त की ओर सामान्य
- – विशिष्ट की ओर सूक्ष्म
- – स्थूल की ओर अज्ञात
- – ज्ञात की ओर
- — निगमन प्रणाली को सूत्र विधि, सिद्धांत प्रणाली व पाठ्य पुस्तक प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है।
- — निगमन विधि शिक्षक केन्द्रित विधि है।
- — हिंदी व्याकरण की सर्वोत्तम विधि – आगमन विधि है।
6. समवाय विधि — समवाय का अर्थ होता है – समूह के साथ – साथ यह विधि पाठ के सभी बिंदुओं को साथ लेकर चलने वाली विधि। इसलिए इसे समवाय विधि कहा जाता है। इस विधि में रचना, कहानी, पद्य आदि की शिक्षा देने के साथ-साथ अवसर के अनुकूल व्याकरण की शिक्षा दी जाती है।
- — भाषा सिखाने के लिए इसे उपयुक्त विधि कहा गया है।
- — इसमें बालक मूल पाठ्यवस्तु से भटक जाता है।
7. सूत्र विधि — यह व्याकरण शिक्षण की प्राचीन विधि है। यह ‘संस्कृत’ से आई है। इसमें बालकों को पहले नियम बताए जाते हैं।- — उन नियमों को सूत्रों में रूपांतरित करके बालकों को उनका बार-बार अभ्यास कराया जाता है।
- — पाणिनी का अष्टाध्यायी सूत्र विधि में है।
- — संस्कृत की प्रसिद्ध पुस्तक सिद्धांत कौमुदी भी सूत्र रूप में पढ़ाई जाती है।
8. भाषा संसर्ग-सह/साथ — संसर्ग का अर्थ – सह/ साथ होता है। इस विधि में बालको को भाषा विशेषज्ञों की पुस्तकों का संसर्ग प्रदान किया जाता है। बालक उनके वातावरण में रहता है, उनके द्वारा उच्चरित भाषा को सुनता है और धीरे-धीरे बालक भी उनकी तरह शुद्ध भाषा बोलना सीख जाता है।
— इस विधि मे वातावरण के अनुसार व्यावहारिक भाषा सीखने पर बल दिया गया है।
— इसमें विशेषज्ञों के संसर्ग की बात कही गई है। लेकिन उनका संसर्ग मिल पाना कठिन होता है।