भाषा– भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की ‘भाष्’ धातु से हुई है जिसका अर्थ होता है – बोलना/कहना। अर्थात् “ध्वनि प्रतीकों के माध्यम से भावों को व्यक्त करना ही भाषा है।” भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरों के विचारों को समझते है।
परिभाषाएँकाव्यदर्श के अनुसार –“यदि संसार में भाषा की ज्योति न होती तो संपूर्ण संसार अंधकारमय हो जाता |
रामचंद्र वर्मा के अनुसार – “मुख से उच्चरित होने वाले वर्णों व शब्दों का समूह जिसके द्वारा मन की बात बतलाई जाती है भाषा कहलाती है”
सुमित्रानंदन पंत के अनुसार – “भाषा ध्वनि का स्वरूप है संपूर्ण विश्व की हृदयतंत्री की झंकार ही भाषा के रूप में अभिव्यक्त की जाती है।” हिंदी शिक्षण के सामान्य उद्देश्य :-
1. हिंदी के वाक्यों, गद्य खंडो व कविताओं को अर्थपूर्ण पढ़ने की योग्यता प्रदान करना।
2. हिंदी कविताओं को भावों के अनुसार पढ़ने की योग्यता प्रदान करना।
3. हिंदी के वाक्यों, गद्य खंडो व कविताओं को अर्थपूर्ण पढ़ने की योग्यता प्रदान करना।
4. भाषा के ध्वनि तत्त्वों से बालकों का परिचित कराना।
5. विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करना।
6. समाजिक एकता व राष्ट्रीय एकता का विकास करना।
7. हिंदी भाषा के प्रति प्रेम उत्पन्न करना।
नोट – माध्यमिक बोर्ड के सेवानिवृत सचिव श्री तेजकरण इंडिया ने बालको के सलेख को सधारने के लिए एक योजना चलाई और इस योजना का नाम – “सुलेख लेखन की प्यास जगाओ” है।
सुलेख– सुलेख का अर्थ शब्दों को सुंदर लिखने से होता है। इसमें बालकों को केवल एक ही वर्ण लिखने के लिए कहा जाता है लेकिन वह सुंदर होना चाहिए। सुलेख लिखते समय आंखों से अभ्यास पुस्तिका की दूरी एक-सवा फुट होनी चाहिए। कलम की लंबाई बालक के एक बालिस्त के बराबर होनी चाहिए। कलम का पृष्ठ भाग तर्जनी अंगुली से 60° के कोण पर झुका हुआ होना चाहिए।
अनुलेख – अनुलेख को सुलेख का ही पर्यायवाची कहा जाता है। इसमें भी बालकों से सुंदर शब्दों को लिखने के लिए कहा जाता है, लेकिन देख-देख कर।
प्रतिलेख – इसमें बालकों को किसी पत्रिका, पुस्तक आदि में से गद्यांश की कुछ पंक्तियों को लिखने के लिए कहा जाता है। प्रतिलेख में अध्यापक को यह ध्यान रखना चाहिए कि दिया जाने वाला
प्रतिलेख – बालकों की रूचि और स्तर के अनुरूप होना चाहिए।
श्रुतिलेख – श्रुतिलेख का अर्थ सुनकर लिखने से है।श्रुतिलेख के माधयम से बालकों की श्रवण शक्ति का विकास किया जाता है।
1. किसी भाषा को सीखने के लिए 4 अवयवों का निश्चित क्रम है
(1) जिज्ञासा, प्रयत्न, अनुकरण, अभ्यास
(2) अभ्यास, जिज्ञासा, अनुकरण, प्रयत्न
(3) जिज्ञासा, अनुकरण, प्रयत्न, अभ्यास
(4) प्रयत्न, अनुकरण, जिज्ञासा,
अभ्यास भाषा की विशेषताएँ और प्रकृति
1. भाषा का एक मानक रूप होता है।
2. भाषा अर्जित संपत्ति है।
3. भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है।
4. भाषा सतत् परिवर्तनशील प्रक्रिया है।
5. भाषा अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती है।
6. प्रत्येक भाषा का भौगोलिक व ऐतिहासिक स्वरूप भिन्न-भिन्न होता है।
7. एक भाषा की संरचना दूसरी भाषा से अलग होती है।
8. भाषा कठिनता से सरलता की ओर होती है।
9. भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं।
10. भाषा एक परंपरा है इसे अर्जित तो किया जा सकता है, परन्तु उत्पन्न नहीं किया जा सकता है।
11. भाषा स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ती है।
हिंदी भाषा शिक्षण की आवश्यकता क्यो?
– चारों कौशलों का विकास करने के लिए।
– सौंदर्य अनुभूति की प्राप्ति करने के लिए।
– ज्ञान की प्राप्ति व ज्ञान को स्थायित्व प्रदान करने के लिए।
– बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए।
हिंदी भाषा शिक्षण की चुनौतियां
1. कुशल अध्यापकों का अभाव ।
2. हिंदी भाषा में नवीन शिक्षण विधियों का अभाव ।
3. भाषा में सहायक उपागमों का अभाव ।
4. विदयालयों में भाषा प्रयोगशाला का अभाव।
5. हिंदी भाषा के प्रति बालकों का कम रूझान ।
6.हिंदी विषय के अतिरिक्त अन्य विषयों में बालकों का रूझान ।
7. शुद्ध लेखन व उच्चारण की समस्या।
8. आगामी समय में उन्नति का अभाव ।
समाधान –
1. अध्यापक को भाषा सिखाने में दक्षता लानी चाहिए और बालकों में रुचि उत्पन्न करनी चाहिए।
2. हिंदी भाषा में सहायक सामग्री का प्रयोग करके भी भाषा शिक्षण को रूचिकर बनाया जा सकता है।
भाषा दक्षता का विकास
1. बालक जिस समाज में रहता है उसमें बोली जाने वाली भाषा को सुनता है।
2.जैसी भाषा सुनता है वैसी ही भाषा बोलता है।
3. बालक अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए भाषा को सीखता है।
4. भाषा को सिखने के लिए उसकी जिज्ञासा पूरी हो जाती है।
5. जिज्ञासा को पूरा करने के लिए बालक के द्वारा पहले प्रयत्न किए गए उसके बाद अनुकरण व अभ्यास के माध्यम से सीखा गया।
भाषा दक्षता के विकास की प्रक्रिया अथव भाषा सीखने का मानोविज्ञान
1. बालक सबसे पहले किसी भी वस्तु को देखता है, देखने से उसके मस्तिष्क में दृष्टि बिंब बनता है।
2. अलग-अलग लोगों के द्वारा उस वस्तु का नाम दिए जाने पर बालक के मस्तिष्क में श्रुति बिंब बनता है।
3. दृष्टि बिंब व श्रुति बिंब दोनों के बनने के बाद बालक के मस्तिष्क में उस वस्तु का प्रत्यय बनता है।
4. फिर बालक उस वस्तु की अनुपस्थिति में भी उसके बारे में सोचने व मनन करने लगता है। यही विचार बिंब व भाव बिंब का निर्माण करते हैं।
A. दृष्टि बिंब B. श्रुति बिंब C. विचार बिंब D. भाव बिंब
5. जब बालक ने पहली बार पानी को देखा तो बालक के मस्तिष्क में उसका दृष्टि बिंब बना। लोगों के द्वारा उसका नाम पुकारने पर बालक के मस्तिष्क में श्रृति बिंब बना। पानी को पीने पर बालक की प्यास बुझी तो उसे विचार आया कि पानी प्यास बुझाता है और इस प्रकार उसमें विचार बिंब का निर्माण हुआ। पानी अच्छा होता है इससे भाव बिंब का निर्माण हुआ।
2. शिक्षण विधियाँ
— शिक्षण में विधियाँ शब्द का प्रयोग अध्यापक की उन प्रक्रियाओं के लिए किया जाता है, जिनकी सफलता पूर्ण समाप्ति के फलस्परूप अर्थात् परिणामस्वरूप बालक कुछ सीखता है और जिनके द्वारा शिक्षण कार्य को बालकों के लिए प्रभावी व रोचक बनाया जाता है। — शिक्षण विधियाँ सीखने का एक साधन है। — श्रीमती एस.के.कोचर ने अपनी पुस्तक Methods & Techniiques of Teaching में शिक्षण विधियों के महत्त्व की अत्यन्त सुंदर व्याख्ता प्रस्तुत की है वह लिखती है – “जिस प्रकार एक सैनिक को हथियारों का ज्ञान होना अत्यन्त आवश्यक होता है उसी प्रकार एक शिक्षक को भी शिक्षण विधियों का ज्ञान होन अत्यन्त आवश्यक है। किस समय कौनसी विधि का प्रयोग किया जाए यह अध्यापक की निर्णय शक्ति पर निर्भर करता है।”
गद्य शिक्षण
1. गद्य शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की गद् धातु से हुई है जिसका अर्थ होता है – स्पष्ट करना। गद्य शिक्षण का उद्देश्य छात्रों में पठन की योग्यता का विकास करना है।
2. गद्य को ‘कवियों की कसौटी’ कहा जाता है।3. इसे English में Prose कहा जाता है।
गद्य शिक्षण की मुख्य विधियाँगद्य शिक्षण की मुख्य रूप से दो विधियाँ –
1. अर्थबोध विधि 2. आदर्श विधि
1. अर्थ बोध विधि — यह अमनोवैज्ञानिक विधि है इस विधि में अध्यापक कक्षा में आता है। पाठ्यपुस्तक को हाथ में लेकर शब्दों के अर्थ बताता है व व्याख्या करता है। इस विधि में बालकों की रूचि का कोई ध्यान नहीं रखा जाता है। इस विधि के माध्यम से पाठयक्रम को तो पूर्ण कराया जा सकता है और कक्षा में उत्तीर्ण भी हुआ जा सकता है। परंतु इससे बालक को कोई विशेष लाभ नहीं पहुंचता है अर्थात् बालक का सर्वांगीण विकास नहीं होता है।– इससे स्थाई ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसे पढ़ते हैं।
2. आदर्श विधि – यह मनोवैज्ञानिक विधि है इस विधि में बालकों की रूचि का ध्यान रखा जाता है और उनका सर्वांगीण विकास किया जाता है। आदर्श विधि में ‘हरबर्ट स्पेन्सर’ की पंचपदीय प्रणाली के माध्यम से शिक्षण कार्य कराया जाता है। इसे पढ़ाया जाता है।
स्पेन्सर के पाँच पद (पंचपदीय) निम्नलिखित है –
1. प्रस्तावना 2. प्रस्तुतीकरण 3. व्यवस्था 4. तुलना 5. सामान्यीकरण
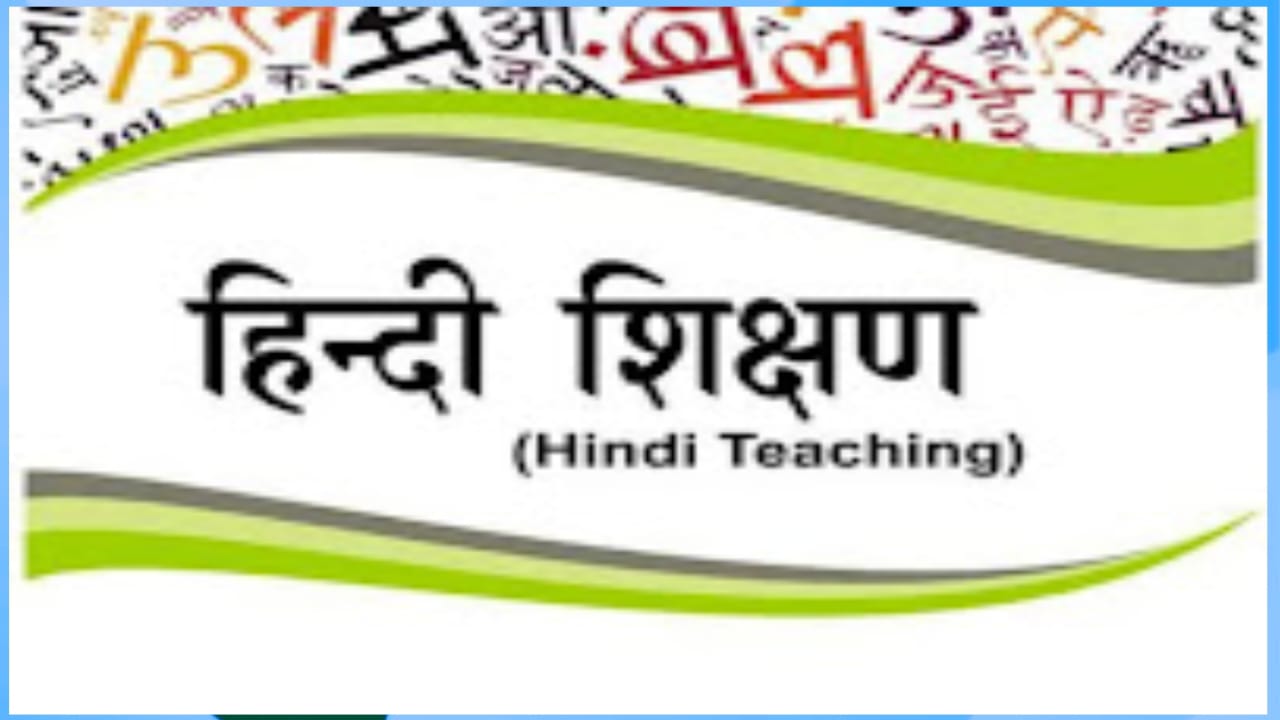
1 thought on “हिंदी शिक्षण विधियां – नोट्स 1”